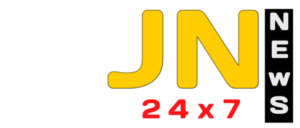माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) भारत सरकार का एक अधिनिय है जो वृद्ध व्यक्तियों एवं माता-पिता के भरण-पोषण एवं देखरेख का एक प्रभावी व्यवस्था करती है। इसका विधेयक सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था।
अधिनियम के मुख्य प्रावधान
(१) वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।
(२) ‘अभिभावक’ में सगे और दत्तक माता पिता और सोतेले माता और पिता सम्मिलित हैं।
(३) प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबधितों से भी भरणपोषण की माँग कर सकता है, जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
(३) वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संगीन अपराध है, जिसके लिये रुपये 5000/- का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।
(४) अधिकरण द्वारा मासिक भरणपोषण हेतु अधिकतम राशि रुपये 10,000/- प्रतिमाह तक का, आदेश किया जा सकता है।
(५) सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जायेगा तथा चिकित्सालयों में विद्गोष पंक्तियों का प्रबंध किया जायेगा।
वर्ष 2007 के अधिनियम में संशोधन हेतु निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं:
पारिवारिक संरचना में बदलाव:
वर्तमान में एकल परिवारों (Nuclear Families) का प्रचलन बढ़ रहा है तथा पारंपरिक संयुक्त परिवारों (Joint Families) की संरचना में बदलाव हुआ है। इस वजह से वृद्धावस्था में अधिकांश लोगों को अकेले रहना पड़ता है जिससे वरिष्ठ नागरिकों की अवहेलना, उनके प्रति अपराध, उनके शोषण तथा परित्याग आदि के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018 में जारी रिपोर्ट (National Crime Record Bureau- NCRB) के अनुसार, वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2018 में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध के मामलों में 13.7% की वृद्धि हुई है।
वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में बढ़ोतरी:
भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1951 में 2 करोड़ थी जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 10.4 करोड़ हो गई।
यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार, भारत में वर्ष 2025 तक यह संख्या दोगुनी हो जाएगी।
वृद्धाश्रमों की स्थिति तथा अवहनीय स्वास्थ्य सुविधाएँ:
वर्तमान में उपलब्ध वृद्धाश्रमों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिये पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं।
इसके अलावा वृद्धाश्रमों का रखरखाव न होने तथा अस्पतालों में जराचिकित्सा (Geriatric) की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है।
संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन:
वृद्धजनों के लिये बुनियादी सुविधाओं जैसे- भोजन, स्वास्थ्य, घर तथा अन्य आवश्यकताओं की अनुपलब्धता उनके मानवाधिकारों का हनन करता है।
यह संविधान के अनुच्छेद-21, जो कि प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण तथा स्वतंत्र जीवन जीने की अधिकार देता है, का हनन है।
न्यायालय का आदेश:
सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा ये आदेश जारी किये गए हैं कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों की समीक्षा की जाए।
प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं:
परिभाषा (Definition):
अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की परिभाषा में (नाबालिग बच्चों को छोड़कर) बच्चे और नाती-पोते शामिल हैं, जबकि विधेयक इस परिभाषा में सौतेले पुत्र, दत्तक पुत्र (जिन्हें गोद लिया गया है), पौत्र, पौत्री, बहू, दामाद को शामिल करता है। इसके अलावा यह विधेयक नाबालिग बच्चों के वैधानिक अभिभावक को भी इसमें शामिल करता है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम के अनुसार संबंधी का अर्थ किसी संतानरहित वरिष्ठ नागरिक के वैधानिक उत्तराधिकारी से है जिसके पास उस वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति है या उसकी मृत्यु के बाद विरासत में मिलेगी। इसमें नाबालिग बच्चे शामिल नहीं हैं, जबकि विधेयक में नाबालिग बच्चों को भी शामिल किया गया है जिनका प्रतिनिधित्व उनके वैधानिक अभिभावक करेंगे।
अधिनियम में माता-पिता का अर्थ जैविक, गोद लेने वाले और सौतेले माता-पिता से है, जबकि विधेयक माता-पिता की परिभाषा में सास-ससुर, दादा-दादी और नाना-नानी को भी शमिल करता है।
अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण में भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सीय सहायता और उपचार शामिल हैं, जबकि विधेयक भरण-पोषण में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिये स्वास्थ्य देखभाल, बचाव और सुरक्षा के प्रावधान को भी शामिल करता है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।
अधिनियम के तहत कल्याण में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों के लिये ज़रूरी अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, जबकि विधेयक कल्याण में आवास, कपड़े, सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों या माता-पिता के शारीरिक एवं मानसिक कल्याण के लिये आवश्यक अन्य सुविधाओं को भी शामिल करता है।
भरण-पोषण का आदेश (Maintenance Order):
अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारें भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunal) बनाएंगी ताकि वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को देय भरण-पोषण राशि पर निर्णय किया जा सके। यह अधिकरण बच्चों और संबंधियों को निर्देश दे सकता है कि वे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु 10,000 रुपए का मासिक शुल्क अदा करें।
जबकि विधेयक भरण-पोषण शुल्क की अधिकतम सीमा को हटाता है तथा अधिकरण को इस शुल्क की अधिकतम राशि निर्धारित करने की शक्ति देता है। अधिकरण भरण-पोषण की राशि पर फैसला करने के लिये निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकता है:
माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक का जीवन स्तर और आय।
बच्चों की आय।
अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि वरिष्ठ नागरिक के बच्चे और संबंधी आदेश के 30 दिनों के भीतर संबंधित माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक को भरण-पोषण की राशि दें। विधेयक इस अवधि को 30 दिन से घटाकर 15 दिन करता है।
अपील (Appeals):
अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों या माता-पिता को भरण-पोषण अधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान करता है, जबकि विधेयक बच्चों और संबंधियों को भी अधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील करने की अनुमति देता है।
अपराध और सज़ा (Offences and Penalties):
अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता को त्यागने पर तीन महीने की कैद या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है, जबकि विधेयक कैद की अवधि को तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने और जुर्माने की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 10,000 रुपए करता है या दोनों सज़ाएँ साथ-साथ भुगतनी पड़ सकती हैं।
विधेयक में यह प्रावधान भी है कि अगर बच्चे या संबंधी भरण-पोषण के आदेश का अनुपालन नहीं करते तो अधिकरण देय राशि की वसूली के लिये वारंट जारी कर सकता है। इसके साथ ही जुर्माना न चुकाने की स्थिति में एक महीने तक की कैद या जब तक जुर्माना नहीं चुकाया जाता तब तक की कैद हो सकती है।
भरण-पोषण अधिकारी (Maintenance Officer):
अधिनियम में प्रावधान है कि अधिकरण की कार्यवाही के दौरान माता-पिता का प्रतिनिधित्व भरण-पोषण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जबकि विधेयक के अंतर्गत भरण-पोषण अधिकारी से निम्नलिखित को सुनिश्चित कराना अपेक्षित है:
भरण-पोषण के भुगतान से संबंधित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना।
माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों के लिये संपर्क सूत्र का काम करना।
देखभाल-गृह की स्थापना (Establishment of care-homes):
अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार वृद्धाश्रम बना सकती है। विधेयक इस प्रावधान को हटाता है और वरिष्ठ नागरिकों के लिये देखभाल-गृह का प्रावधान करता है जिन्हें सरकार या निजी संगठन द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
इन गृहों का पंजीकरण राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण में कराना होगा। केंद्र सरकार इन गृहों के लिये भोजन, चिकित्सा सुविधा और अन्य अवसंरचनाओं से संबंधित न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करेगी।
स्वास्थ्य देखभाल (Healthcare):
अधिनियम सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिये कुछ सुविधाओं का प्रावधान करता है जैसे- अलग पंक्ति, बिस्तर और जरारोग (Geriatric) के मरीज़ों के लिये सुविधाएँ आदि।
प्रस्तावित विधेयक में निजी संगठनों सहित सभी अस्पतालों से भी अपेक्षा की गई है कि वे वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी सभी सुविधाएँ प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त विकलांग वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
सुरक्षा और कल्याण संबंधी उपाय (Protection and welfare measures): विधेयक में प्रत्येक पुलिस स्टेशन से अपेक्षा की गई है कि उसका कम-से-कम एक अधिकारी, जो कि सहायक उप-निरीक्षक (Assistant Sub-Inspector) से निचले पद का न हो, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों का निपटारा करेगा।
इसके अलावा विधेयक में राज्य सरकारों को निर्दिष्ट किया गया है कि वे प्रत्येक ज़िल
में वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक विशेष पुलिस इकाई की स्थापना करें तथा उस इकाई का प्रमुख पुलिस उप-अधीक्षक (Deputy-Superintendent of Police) या उससे उच्च पद का अधिकारी होगा।
विधेयक में निम्नलिखित समस्याएँ निहित हैं:
मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी: यह विधेयक वरिष्ठ नागरिकों तथा वृद्धजनों में होने वाली मानसिक समस्याओं जैसे- अवसाद (Depression), स्मृतिभ्रम (Dementia) तथा अल्ज़ाइमर रोग (Alzheimer’s Disease) की उपेक्षा करता है जो कि भारत में एक गंभीर समस्या है।
ऐजवेल फाउंडेशन (Agewell Foundation) के अनुसार, वर्ष 2017-18 में भारत के प्रत्येक दो वृद्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है जिससे अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
वृद्ध महिलाओं की समस्या: वर्ष 2011 की जनसंख्या के आँकड़ों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों में लिंगानुपात 1033 है जो कि वर्ष 1971 में 938 था। इनमें अधिकांश संख्या विधवा तथा अत्यधिक आश्रित वृद्ध महिलाओं की है। विधेयक में इन महिलाओं की समस्या तथा इनकी विशेष आवश्यकताओं के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
जागरूकता हेतु प्रयास नहीं: वर्तमान में अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हैं तथा उन्हें नहीं पता कि वे अपने बच्चों और संबंधियों द्वारा उनके प्रति किये जाने वाले अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं।
देखभाल गृहों की समस्या: वर्तमान में देश के अधिकांश देखभाल गृहों में शुल्क का भुगतान करके रहने की व्यवस्था होती है। इन परिस्थितियों में उन वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी कोई संतान या रिश्तेदार नहीं हैं या जिन्होंने कोई संपत्ति नहीं एकत्रित की है, की देखभाल के लिये कोई स्थान नहीं होगा।
संभावित सुझाव:
ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जिससे विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रतिधारित (Retain) या नियुक्त (Hire) किया जाए ताकि उनके ज्ञान और अनुभवों का उपयोग हो सके।
प्रौढ़ शिक्षा तथा वृद्धजनों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि उनको जागरूक, सशक्त और स्वायत्त बनाया जा सके। वर्तमान में देश के वरिष्ठ नागरिकों की साक्षरता दर मात्र 44% है।
वरिष्ठ नागरिकों हेतु समुदाय आधारित कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाए जैसा कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (National Health Service) में किया जाता है।
बैंकों की मदद से वरिष्ठ नागरिकों को विशेष ऋण उपलब्ध कराए जाएँ ताकि छोटे व्यवसायों के माध्यम से वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी तथा सुरक्षित हो सकें।
सरकार गरीब तथा बेघर वृद्धजनों हेतु निःशुल्क देखभाल गृहों का निर्माण करे।
वृद्धाश्रमों की स्थिति तथा उनके प्रति लोगों का नज़रिया बदला जाए ताकि वह लोगों की मजबूरी न बनकर उनकी पसंद बनें।
इमानवेल सिंह
अध्यक्ष
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
जनहित में जारी…..